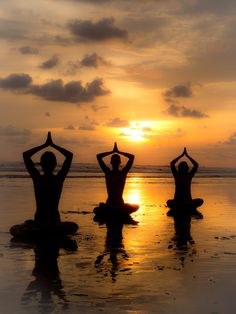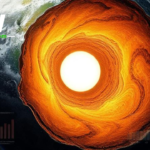सांख्य – योग भारत का सबसे प्राचीन दर्शन है । सांख्य और योग दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं । सांख्य सैद्धांतिक पक्ष है और योग व्यावहारिक पक्ष । सांख्य ज्ञान पक्ष है और योग कर्म पक्ष । श्रीमद्भगवद्गीता में कहा गया है पंडित लोग सांख्य और योग को पृथक नहीं कहते हैं ।
सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।
एकमप्यस्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ।।
सांख्य दर्शन को प्रस्तुत करने वाले कपिल मुनि हैं । बुद्ध की जन्मस्थली कपिलवस्तु का नाम कपिल मुनि के नाम पर ही है । पुराणों में कपिल मुनि को विष्णु के 24 अवतारों में से एक माना जाता है । महाभिनिष्क्रमण के पश्चात् बुद्ध सर्वप्रथम जिस आचार्य के पास ज्ञान की प्राप्ति हेतु गए थे वे सांख्य शास्त्र के आचार्य अलार कलाम थे । बुद्ध के विचार सांख्य योग पर ही आधारित हैं । सांख्य तीन प्रकार के दुःख बतलाया है – आधिदैविक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक । सारा संसार इन तीनों दुःखों से ग्रसित है । इन दुःखों से मुक्ति पाना ही मनुष्य मात्र का लक्ष्य है । प्रकृति त्रिगुणात्मिका है और प्रकृति के तीनों ही गुण चाहे सत्व गुण हो , रजो गुण हो या तमो गुण ये सभी दुःख के कारण हैं । हम इसे सिगगमंड फ्रायड के इड, इगो तथा सुपरइगो से समझ सकते हैं । सुपरइगो यानी सत्व गुण , इगो यानी रजो गुण और इड यानी तमोगुण तीनों दुःख के कारण हैं । बुद्ध भी कहते हैं – सब्बं दुक्खं । सब कुछ दुःखमय है । सांख्य के अनुसार जड़ प्रकृति और चेतन पुरुष का संबंध ही दुःख का कारण है और दोनों के संबंध का ज्ञान ही दुःख की निवृत्ति अर्थात् मोक्ष की अवस्था । इसके लिए योग उपाय बताता है जिसे हम आष्टांगिक योग के नाम से जानते हैं । ये हैं यम , नियम , आसन , प्रणायाम, प्रत्याहार, धारणा , ध्यान और समाधि । बुद्ध भी दुःखों से पूर्ण रूप से छुटकारे के लिए आष्टांगिक मार्ग के बारे में बताते हैं । वे हैं सम्यक् दृष्टि, सम्यक् संकल्प, सम्यक् वाक्, सम्यक् कर्म, सम्यक् आजीविका, , सम्यक् व्यायाम, सम्यक् स्मृति और सम्यक् समाधि । सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद को मानता है । सांख्य के अनुसार कार्य अपने कारण में विद्यमान है । शून्य से हमेशा शून्य की ही उत्पत्ति होगी । शून्य से कभी भी सृष्टि उत्पन्न नहीं हो सकती । कार्य अपने कारण में स्थित है । श्रीमद्भगवद्गीता के इस श्लोक पर सांख्य के सत्कार्यवाद का साफ साफ प्रभाव देखा जा सकता है ।
नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः।
उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ।।
दुनिया के जितने भी धर्म यथा पौराणिक धर्म, ईसाईयत आदि वे सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं जबकि सांख्य सृष्टि का विकास मानता है । बुद्ध भी यही मानते हैं कि कार्य अपने कारण में विद्यमान है । बिना कारण के कार्य उत्पन्न नहीं होता । यही बुद्ध का प्रतीत्यसमुत्पाद है जो कि संपूर्ण बौद्ध चिंतन का आधार है अगर देखा जाए तो बुद्ध ने एक तरह सांख्य योग का अपनी भाषा में अनुवाद किया है । आधुनिक विज्ञान में भी परमाणु के तीन मूल कणों प्रोटॉन, इलेकट्राॅन तथा न्यूट्रान में प्रकृति के तीनों गुणों सत्व, रज और तम को देख सकते हैं । प्रोटॉन सत्व गुण है , इलेक्ट्राॅन रजो गुण है और न्यूट्रान तमो गुण है । सांख्य कहता है कि रजो गुण प्रकृति को क्रियाशील करता है । आधुनिक विज्ञान में भी हम देखते हैं कि इलेक्ट्राॅनों के कारण ही तत्वों के परमाणु आपस में संयोग करके पदार्थ का निर्माण करते हैं । अगर परमाणु में इलेक्ट्रान , प्रोटान और न्यूट्रान बराबर हो जाएं तो फिर परमाणुओं का संयोग होगा ही नहीं । यही बात सांख्य भी कहता है कि प्रकृति में तीनों गुण जब साम्यावस्था में रहते हैं तो कुछ भी निर्मित नहीं होता । इसी तरह सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद आधुनिक विज्ञान का आधार है । कार्य अपने कारण में विद्यमान है । जिस विकासवाद को डार्विन ने बहुत बाद में प्रस्तुत किया सांख्य उसकी चर्चा बहुत पहले कर चुका है । सांख्य के अनुसार सृष्टि अचानक उत्पन्न नहीं हुई बल्कि उसका विकास हुआ है ।
त्रिगुणात्मिका प्रकृति के सत्व, रज और तम इन तीनों गुणों से निर्मित आधिदैविक, अधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दुःख से निवृत्ति के लिए योग जो हमको रास्ता देता है उसे अष्टांग योग कहते हैं । अष्टांग योग के अंतर्गत यम , नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि क्रियाएं आती हैं ।
यम – यम के अंतर्गत अहिंसा, सत्य , अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य क्रियाएं आती है ।
नियम – नियम के अंतर्गत शौच , संतोष, तप , स्वाध्याय तथा ईश्वर प्राणिधान क्रियाएं आती हैं ।
आसन – पतंजलि के अनुसार ” स्थिरसुखासनम् ‘ । सुखपूर्वक स्थिर बैठना आसन कहलाता है । जिसने भी योगासन के नाम पर किए जाने वाले आसन हैं वे हठयोग के आसन हैं न कि पतंजलि के । पतंजलि के अनुसार सुखपूर्वक बैठने की स्थिति ही आसन है ।
प्रणायाम – प्रणायाम का अर्थ होता है पंच प्राणों पर नियंत्रण। प्राण हमको संचालित करते हैं । लेकिन जब हम प्राणों से संचालित न होकर पंच प्राणों पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं तो इसी को प्रणायाम कहते हैं ।
प्रत्याहार – जो हमारी इंद्रियां वासनाओं की तरफ दौड़ती हैं उन्हें खींचकर अपने भीतर स्थित कर लेना प्रत्याहार है ।
यथा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ।।
धारणा – एकाग्रता प्राप्त करने को धारणा कहते हैं ।
ध्यान – विशुद्ध चैतन्य स्थिति को प्राप्त करने को ध्यान कहते हैं ।
समाधि – मन की पूर्ण शांति ही समाधि है । जब इंद्रियों अपने विषयों से हटकर स्वयं में लीन हो जाती हैं और व्यक्ति जब रस , रुप, गंध, स्पर्श और शब्द से हटकर पूर्णतः शांति को प्राप्त कर लेता है तो इसे ही पुरुष को प्रकृति के तीनों गुणों से रहित होने की स्थिति कहते हैं और यही समाधि है ।
कुल मिलाकर योग हमारे मानसिक कचरे को बाहर निकालने का साधन है । ये मानसिक कचरे हैं – काम , क्रोध, लोभ , मोह , ईर्ष्या , राग – द्वेष । इन मानसिक कचरों से हम अपने सत् चित् और आनंद से परिपूर्ण जीवन को दुःखों का घर बना लेते हैं । मानसिक कचरा ही इस संसार में संपूर्ण दुःख का कारण है । अपने मानसिक कचरे को निकालकर मनुष्य के जीवन से दुःख का समापन और आनंद का आविर्भाव हो जाता है । यही योग है ।
अविनाश चंद्र
प्रवक्ता ( हिंदी)
अटल उत्कृष्ट राजकीय इंटरमीडिएट काॅलेज बिलखेत पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड ।