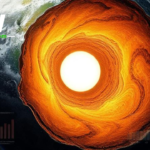वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की 70वीं बैठक में ‘2030 सतत विकास हेतु एजेंडा’ के तहत सदस्य देशों द्वारा 17 विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals – SDGs) और 169 प्रयोजन अंगीकृत किए गए। यह लक्ष्य वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता को बढ़ावा देने के लिए तय किए गए हैं।
क्या है सतत विकास?
‘पर्यावरण और विकास पर विश्व आयोग’ (1983) के अंतर्गत बर्टलैंड कमीशन द्वारा जारी रिपोर्ट (1987) के अनुसार, “आने वाली पीढ़ी की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास ही सतत विकास है।”
सतत विकास: वर्तमान और भविष्य के बीच संतुलन
सतत विकास वह विकास है जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह एक दृष्टिकोण है जो समाज की विभिन्न, और अक्सर प्रतिस्पर्धी, आवश्यकताओं के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। इसमें पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक सीमाओं के प्रति जागरूकता का समावेश है।
अक्सर, विकास किसी एक विशेष आवश्यकता से प्रेरित होता है, बिना व्यापक या भविष्य के प्रभावों पर पूरी तरह विचार किए। हम पहले से ही देख रहे हैं कि इस तरह के दृष्टिकोण से कितना नुकसान हो सकता है, जैसे गैर-जिम्मेदार बैंकिंग के कारण बड़े पैमाने पर वित्तीय संकट या जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा स्रोतों पर हमारी निर्भरता के परिणामस्वरूप वैश्विक जलवायु में परिवर्तन।
असंघारणीय विकास को जारी रखने से इसके परिणाम और भी गंभीर और लगातार होते जाएंगे, यही कारण है कि हमें अभी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। सतत विकास की अवधारणा की व्याख्या कई अलग-अलग तरीकों से की जा सकती है, लेकिन इसके मूल में यह विकास के लिए एक दृष्टिकोण है जो विभिन्न आवश्यकताओं और सीमाओं को संतुलित करने का प्रयास करता है।
सतत विकास का लक्ष्य है कि हम अपने संसाधनों का उपयोग इस प्रकार करें कि वे हमारे भविष्य को खतरे में न डालें। यह एक समग्र दृष्टिकोण है जो दीर्घकालिक विचारों को ध्यान में रखता है और विभिन्न कारकों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है ताकि हम एक बेहतर और अधिक संतुलित भविष्य की ओर बढ़ सकें।
SDGs क्यों?
MDGs (Millennium Development Goals) की अवधि 2015 में समाप्त हो गई। इन लक्ष्यों ने मानव विकास को प्राथमिकता दी, लेकिन पर्यावरण सुरक्षा को पर्याप्त महत्व नहीं दिया। इसलिए, SDGs को इस उद्देश्य से स्थापित किया गया कि वे पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ मानव विकास को भी ध्यान में रखें।

संयुक्त राष्ट्र का एजेंडा 2030: 17 विकास लक्ष्य
- गरीबी के सभी रूपों की समाप्ति।
- भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा।
- सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य, सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा।
- समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तायुक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ सभी को सीखने का अवसर देना।
- लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करना।
- सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- सस्ती, विश्वसनीय, टिकाऊ और आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच सुनिश्चित करना।
- सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्य को बढ़ावा देना।
- लचीले बुनियादी ढाँचे, समावेशी और सतत औद्योगीकरण को बढ़ावा देना।
- देशों के बीच और भीतर असमानता को कम करना।
- सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण।
- स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना।
- जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई करना।
- स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग।
- सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिकीय प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव-विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना।
- सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना।
- सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनर्जीवित करना और कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत बनाना।
लक्ष्य 13: जलवायु परिवर्तन से निपटने की कार्रवाई
जलवायु परिवर्तन आज के युग की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके प्रभाव पहले से ही दुनिया भर में दिखाई दे रहे हैं। तापमान में वृद्धि, मौसम के चरम घटनाएँ, बाढ़, सूखा, और समुद्र का स्तर बढ़ना इस संकट के स्पष्ट संकेत हैं। गोल 13 का उद्देश्य इन प्रभावों से निपटने के लिए तत्काल और प्रभावी कार्रवाई करना है। इसमें जलवायु से संबंधित जोखिमों को कम करने, अनुकूलन योजनाएँ विकसित करने, और जलवायु संकट के खिलाफ सामूहिक वैश्विक प्रयासों को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।
जलवायु परिवर्तन और उसके भयंकर प्रभावों का सामना करते देश
आज की दुनिया में कोई भी देश ऐसा नहीं है जो जलवायु परिवर्तन के भयंकर प्रभावों से अछूता हो। 1990 की तुलना में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ गया है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हमारे जलवायु तंत्र में दीर्घकालिक परिवर्तन ला रही है, जिसके परिणामस्वरूप यदि समय पर कदम नहीं उठाए गए, तो अपरिवर्तनीय परिणामों का खतरा बढ़ सकता है।
जलवायु संबंधी आपदाओं से होने वाला वार्षिक औसत आर्थिक नुकसान सैकड़ों अरब डॉलर में है। यह भू-भौतिकीय आपदाओं के मानवीय प्रभावों का भी उल्लेख नहीं करता, जिनमें से 91 प्रतिशत जलवायु से संबंधित हैं। 1998 से 2017 के बीच इन आपदाओं के कारण 1.3 मिलियन लोगों की मौत हुई और 4.4 बिलियन लोग घायल हुए।
विकासशील देशों की जलवायु परिवर्तन के अनुकूल होने और कम कार्बन विकास में निवेश करने की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2020 तक सालाना 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया था। कमजोर क्षेत्रों का समर्थन करना न केवल सतत विकास लक्ष्य 13 में बल्कि अन्य सतत विकास लक्ष्यों में भी सीधे योगदान देता है। इन कार्रवाइयों को राष्ट्रीय विकास रणनीतियों में आपदा जोखिम उपायों, टिकाऊ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन और मानव सुरक्षा को एकीकृत करने के प्रयासों के साथ-साथ चलना चाहिए।
मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, बढ़े हुए निवेश और मौजूदा तकनीक का उपयोग करके, वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि को पूर्व-औद्योगिक स्तरों से दो डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना अभी भी संभव है। इसका लक्ष्य 1.5 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके लिए तत्काल और महत्वाकांक्षी सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है। इस दिशा में सभी देशों को मिलकर प्रयास करने होंगे ताकि हमारे ग्रह को सुरक्षित और स्वस्थ बनाया जा सके
क्या थे MDGs (Millennium Development Goals)?
MDGs, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2000 में स्वीकार किए गए थे। इन लक्ष्यों की गणना 1990 के स्तर पर की गई थी और ये 2015 तक के लिए थे। इसके अंतर्गत 8 लक्ष्य और 18 उद्देश्य थे।
यूएनडीपी की भूमिका
SDG1 जनवरी 2016 से प्रभाव में आए और यूएनडीपी (United Nations Development Programme) की निगरानी व संरक्षण में अगले 15 वर्षों तक प्रभावी रहेंगे। यूएनडीपी का प्रमुख लक्ष्य है इन देशों में गरीबी को समाप्त करना, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को प्रोत्साहित करना, पर्यावरण परिवर्तन और आपदा परिवर्तन पर कार्य करना और आर्थिक समानता प्राप्त करना।
सतत विकास लक्ष्यों का मुख्य उद्देश्य विश्व से गरीबी को पूर्णतः समाप्त करना और सभी समाजों में सामाजिक न्याय व पूर्ण समानता स्थापित करना है। भारत को भी गंभीरता से इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कार्य करना चाहिए। यह आवश्यक है कि सभी देश इन लक्ष्यों की गंभीरता को समझें और अपने प्रयासों का मूल्यांकन करें, ताकि हम एक समृद्ध, सुरक्षित और न्यायपूर्ण विश्व का निर्माण कर सकें।
अपनी पर्यावरणीय सीमाओं के भीतर रहना सतत विकास के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक है। ऐसा न करने का एक परिणाम जलवायु परिवर्तन है।
लेकिन सतत विकास का ध्यान सिर्फ़ पर्यावरण तक ही सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य एक मज़बूत, स्वस्थ और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करना भी है। इसका मतलब है मौजूदा और भविष्य के समुदायों में सभी लोगों की विविध ज़रूरतों को पूरा करना, व्यक्तिगत कल्याण, सामाजिक सामंजस्य और समावेश को बढ़ावा देना और समान अवसर पैदा करना। सतत विकास का मतलब है भविष्य और वर्तमान दोनों के लिए काम करने के बेहतर तरीके खोजना। हमें अपने काम करने और जीने के तरीके को बदलने की जरूरत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमारे जीवन की गुणवत्ता कम हो जाएगी।
सतत विकास उन मुद्दों पर बेहतर निर्णय लेने का एक तरीका प्रदान करता है जो हमारे सभी जीवन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, नए समुदायों की योजना में स्वास्थ्य योजनाओं को शामिल करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि निवासियों को स्वास्थ्य सेवा और अवकाश सुविधाओं तक आसान पहुँच हो। (अधिक टिकाऊ खाद्य आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रोत्साहित करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि यूके के पास दीर्घकालिक भविष्य के लिए पर्याप्त भोजन हो।
source- undp website, SDG