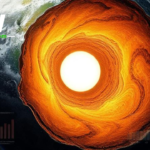मानसून की बारिश: बदलते पैटर्न
भारत में मानसून की बारिश का आगमन सदियों से कृषि, जल संरक्षण और सामान्य जीवन के लिए महत्वपूर्ण रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में मानसून के पैटर्न में काफी बदलाव देखा जा रहा है। ये बदलाव न केवल किसानों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो रहे हैं, बल्कि पूरे देश के पर्यावरण और जलवायु पर भी प्रभाव डाल रहे हैं।
बदलते पैटर्न
- देरी से आगमन: पहले मानसून की बारिश जून के पहले सप्ताह में शुरू हो जाती थी, लेकिन अब इसका आगमन देरी से हो रहा है। इस साल भी मानसून ने सामान्य से लगभग दो सप्ताह बाद दस्तक दी।
- अनियमितता: पहले के मुकाबले बारिश की मात्रा और समय में काफी अनियमितता देखी जा रही है। कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक बारिश हो रही है, जबकि अन्य क्षेत्रों में सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है।
- कम अवधि में अधिक बारिश: मानसून की अवधि में कमी आ रही है, लेकिन इस दौरान भारी बारिश हो रही है। इससे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जो जनजीवन और फसलों को नुकसान पहुंचा रही है।
- क्षेत्रीय असमानता: भारत के विभिन्न हिस्सों में मानसून का प्रभाव भिन्न-भिन्न हो रहा है। उत्तर भारत में जहां भारी बारिश हो रही है, वहीं दक्षिण भारत के कई हिस्सों में सूखा पड़ रहा है।
बदलते पैटर्न के कारण
- जलवायु परिवर्तन: वैज्ञानिकों के अनुसार, जलवायु परिवर्तन का सीधा प्रभाव मानसून पर पड़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्र का तापमान बढ़ रहा है, जिससे मानसून की प्रणाली प्रभावित हो रही है।
- वनीकरण और पर्यावरणीय असंतुलन: वनों की कटाई और शहरीकरण से पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है, जो मानसून के पैटर्न में बदलाव का एक प्रमुख कारण है।
- प्रदूषण: वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन से भी मानसून प्रभावित हो रहा है। इससे न केवल वर्षा का पैटर्न बदल रहा है, बल्कि इसकी गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ रहा है।
प्रभाव
- कृषि पर प्रभाव: अनियमित मानसून के कारण किसानों को फसलों की बुवाई और कटाई में कठिनाई हो रही है। इससे फसल उत्पादन में कमी आ रही है और किसानों की आर्थिक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है।
- जल संकट: भारी बारिश के बावजूद जल संचयन की उचित व्यवस्था न होने से जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। कई क्षेत्रों में भूजल स्तर गिरता जा रहा है।
- बाढ़ और सूखा: एक ही समय में देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और कुछ हिस्सों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है और विस्थापन की स्थिति उत्पन्न हो रही है।
समाधान
- जलवायु अनुकूलन: जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए सरकार और समाज को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। इसके लिए नीतिगत बदलाव और जनजागरूकता अभियान चलाने होंगे।
- वनीकरण: अधिक से अधिक पेड़ लगाने और वनों की रक्षा करने की दिशा में कदम उठाए जाने चाहिए। इससे पर्यावरणीय संतुलन बहाल होगा और मानसून की प्रणाली स्थिर हो सकेगी।
- जल संचयन: वर्षा जल संचयन की उचित व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि जल संकट की स्थिति से निपटा जा सके।
- प्रदूषण नियंत्रण: वायु प्रदूषण और ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए कठोर कदम उठाने होंगे।
मानसून की बारिश: बदलते पैटर्न और बढ़ती चुनौतियाँ
बदलते मानसून के पैटर्न को समझकर और उचित कदम उठाकर ही हम इसके प्रभावों से निपट सकते हैं। इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ भी मानसून की बारिश का सही लाभ उठा सकें।
मानसून का आगमन इस साल भी लोगों के लिए राहत का कारण बना है, लेकिन बारिश के पैटर्न में हो रहे बदलाव ने चिंता की लकीरें खींच दी हैं। हाल के वर्षों में कम समय में अधिक बारिश का पैटर्न देखने को मिल रहा है। देश के अधिकांश हिस्सों में साल भर की बारिश एक दिन, एक हफ्ते या कुछ घंटों में हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या यह मानव जनित बदलाव है या पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया?
- कम समय में अधिक बारिश – बढ़ती बारिश से आम लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, लेकिन उन्हें अल नीनो प्रभाव, पश्चिमी विक्षोभ, चक्रवाती परिसंचरण, मानसून टर्फ, एरोग्राफिक लिफ्टिंग जैसे तकनीकी कारकों के बारे में जानकारी नहीं होती। जलवायु वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में इस मौसम में भारी बारिश के दिन बढ़ेंगे और इसकी आवृत्ति साल दर साल बढ़ती जाएगी।
- मानव जनित जलवायु परिवर्तन – जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल की रिपोर्ट बताती है कि 1950 के बाद से दुनिया भर में भारी बारिश की घटनाओं में वृद्धि हुई है। एक अध्ययन के अनुसार, पिछले 10 वर्षों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान देश के 55 प्रतिशत हिस्से में बारिश बढ़ी है, जबकि 11 प्रतिशत क्षेत्र में बारिश कम हुई है। पर्यावरणविदों का कहना है कि यह बदलाव मानव जनित जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हो रहा है।
- वायुमंडलीय नमी और तापमान – नासा ने दो साल पहले बताया था कि पृथ्वी के तापमान में हर एक डिग्री की वृद्धि से वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा लगभग सात प्रतिशत बढ़ जाती है। इससे कम समय में भारी बारिश की संभावना बढ़ जाती है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार, वर्ष 1901-2018 के दौरान देश में सतही वायु तापमान में 0.7 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है, जिससे वायुमंडलीय नमी भी बढ़ी है।
- महासागरों का बढ़ता तापमान – 1951-2015 के दौरान हिंद महासागर में समुद्र की सतह के तापमान में एक डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। पहले मानसून के दौरान समुद्र की सतह का तापमान गिरता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा। यह असामान्य तापमान वृद्धि आर्द्रता को बढ़ाकर मानसून के नियमित पैटर्न को बिगाड़ देती है।
- पहाड़ी क्षेत्रों में असर – ग्लोबल वार्मिंग के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में वायुमंडल की नमी बढ़ जाती है। इस नम हवा को पहाड़ियों द्वारा ऊपर उठाया जाता है, जिससे भारी बारिश और भूस्खलन जैसी समस्याएं होती हैं। चक्रवाती परिसंचरण और मानसून टर्फ भी भारी बारिश का कारण बनते हैं।
- समाधान की दिशा में कदम – जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए देश को अपना हरित आवरण बढ़ाना होगा और हरित ईंधन पर जोर देना होगा। पर्यावरणीय नियमों का पालन और जनता का सहयोग इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। मौसम विभाग को पूर्वानुमान की सटीकता बढ़ाने के लिए अधिक संसाधनों का निवेश करना होगा। साथ ही, सरकार को जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना को पूरी ईमानदारी से लागू करना होगा।
अनियोजित विकास से तापमान और आर्द्रता में वृद्धि हो सकती है, जिससे अचानक भारी वर्षा की आवृत्ति भी बढ़ सकती है। इससे संबंधित कई परिस्थितियों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन हम सतर्क रहकर और सही कदम उठाकर इसके प्रभावों को कम कर सकते हैं।
source and data – अमर उजाला समाचार पत्र