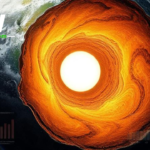जल की आवश्यकता हमारे जीवन के हर पहलू मे हैं चाहे पीने की बात हो या हमारे रोजमर्रा के जीवन मे अलग – अलग जरुरतो को लेकर पानी की माँग । पानी की माँग दिन पर दिन बढ़ती जा रही लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण जलस्रोतों पे बुरा प्रभाव पडा है। भारत में तेजी से बढ़ती आबादी और शहरीकरण ने जल संकट को एक गंभीर समस्या बना दिया है। भारतीय शहरों में पानी की कमी, जल प्रदूषण और अव्यवस्थित जल प्रबंधन जैसे मुद्दे प्रमुख हैं। 2031 तक जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता 1,700 घन मीटर के जल तनाव स्तर से नीचे आने का अनुमान है. इसके परिणामस्वरूप, अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि उत्पादन प्रभावित हो सकता है और इस्पात तथा कोयला बिजली जैसे जल-ग्रहण उद्योग नष्ट हो सकते हैं। UNICEF के अनुसार दुनिया की लगभग दो तिहाई आबादी — हर साल कम से कम एक महीने के लिए गंभीर पानी की कमी का सामना करती है। जल संसाधन मंत्रालय के अनुसार, 2021 में 1,486 क्यूबिक मीटर से 2031 तक भारत में प्रति व्यक्ति औसत वार्षिक जल उपलब्धता 1,367 क्यूबिक मीटर तक घट जाएगी। 1,700 क्यूबिक मीटर से नीचे का स्तर जल तनाव का संकेत है, जबकि 1,000 क्यूबिक मीटर पानी की कमी की सीमा है।
जल संकट के कारण
1. अत्यधिक शहरीकरण: शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती आबादी के कारण जल संसाधनों पर भारी दबाव पड़ा है। नदियों, झीलों और भूजल के अत्यधिक दोहन से जल स्तर में कमी आई है। इस कमी का मुख्य कारण जलस्रोतों का पुनः भंडारण सही से ना होना है । जल्दी शहरीकरण और औद्योगीकरण ने पानी के स्रोतों को दूषित कर दिया है, जिससे वे पीने के लिए अयोग्य हो गए हैं। इसके अलावा, अत्यधिक भूजल निकासी ने महत्वपूर्ण पानी के स्रोतों को खाली कर दिया है। जलवायु परिवर्तन ने संतुलन और बिगाड़ दी है, अनियमित वर्षा पATTERN का कारण बना है और नदियों और कुएं के रिचार्ज को प्रभावित कर रहा है। खराब पानी प्रबंधन और पर्याप्त आधारभूत संरचना की कमी ने भी संकट को और बढ़ा दिया है।
2. जल प्रदूषण: औद्योगिक अपशिष्ट, घरेलू कचरा और कृषि में उपयोग होने वाले रासायनिक पदार्थ नदियों और झीलों को प्रदूषित कर रहे हैं। इससे पीने योग्य पानी की मात्रा घट रही है कभी-कभी किसी इलाके में पानी की कोई कमी नहीं होती लेकिन उस पानी को पीना सुरक्षित है या नहीं, यह दूसरी बात है। दुनिया के कई हिस्सों में सीवेज के लिए खराब सिस्टम हैं – वह पानी जो मानव से प्रभावित है, जैसे घर पर बर्तन धोना या औद्योगिक प्रक्रिया में उपयोग होना। वैश्विक स्तर पर, 44% घरेलू सीवेज का पुनरुपयोग किए ट्रीटमेट के बिना होता है, और बिना संसाधित या पुनरुपयोग किए 80% सीवेज ओवरऑल पारिस्थितिकी में वापस बहता है जिसके अनुसार संयुक्त राष्ट्र के आंकडो के अनुसार 1.8 अरब लोग उसका उपयोग करते हैं जिसके कारण फीकल, रसायन या अन्य दूषक तत्व जहरीले साबित हो सकते हैं। सीवेज दुनिया के सबसे व्यापक रोगों के लिए प्रमुख कारणों में से एक है, जिसमें हैजा, दस्त, टाइफाइड, और पोलियो शामिल हैं।
3. विकास की अव्यवस्थित योजना: बिना उचित योजना के विकास कार्यों से जल संसाधनों का अनियमित उपयोग होता है, जिससे जल संकट बढ़ता है। वर्षाजल संग्रहण, कुशल सिंचाई तकनीकें और जल पुनर्चक्रण स्थायी जल प्रबंधन में योगदान दे सकते हैं। जल संसाधनों के संरक्षण और प्रभावी समाधानों के क्रियान्वयन हेतु समुदाय की जागरूकता और भागीदारी अत्यावश्यकता है ।
प्रभाव
1. स्वास्थ्य समस्याएँ: स्वच्छ पेयजल की कमी से जल जनित बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। यह विशेष रूप से गरीब और वंचित समुदायों में अधिक देखा जाता है। यह जल समस्या विशेष रूप से कई बीमारियों को आमंत्रित करता है जिनसे निपटना काफी मुश्किल हो जाता है । डब्ल्यूडब्ल्यूएफ जल जोखिम फ़िल्टर के परिदृश्यों के अनुसार, जिन 100 शहरों में 2050 तक जल जोखिम में सबसे बड़ी वृद्धि होने की उम्मीद है, वे 350 मिलियन लोगों के घर हैं, और राष्ट्रीय और विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाएं हैं। चीन के लगभग 50 शहर, और भारत के 30 शहर, जिनमें दिल्ली, जयपुर, इंदौर, अमृतसर, पुणे, श्रीनगर, कोलकाता, बेंगलुरु, मुंबई, कोझिकोड और विशाखापत्तनम शामिल हैं, ऐसे उच्च जोखिम वाले क्षेत्र हैं।
2. आर्थिक प्रभाव: जल संकट से कृषि और उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे आर्थिक विकास की गति धीमी हो जाती है। जिसका मुख्य कारण होता है जल की कमी के कारण सिचाई के लिये पानी की कमी जिसके वजह से उत्पादकता मे कमी होती है और खद्य उत्पादों के मुल्य मे वृधि होता है ।
संभावित समाधान
जल संरक्षण के तरीकों को अपनाकर, जैसे वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण से जल संकट को कम किया जा सकता है। साफ सफाई और स्वच्छता से औद्योगिक और घरेलू कचरे के उचित निपटान से जल प्रदूषण को कम किया जा सकता है ।संगठित जल प्रबंध करके जल संसाधनों के उचित प्रबंधन के लिए सरकार और समुदायों के बीच सहयोग आवश्यक है। यह नीतियों और योजनाओं के सही क्रियान्वयन से संभव है।
उदाहरण के लिये बेंगलुरु: यहां भूजल स्तर में गिरावट और झीलों के सूखने की समस्या गंभीर है। दिल्ली: यमुना नदी का जल प्रदूषण उच्चतम स्तर पर है, जिससे शहर को पीने योग्य पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
भारतीय शहरों में जल संकट एक जटिल समस्या है जिसे हल करने के लिए समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है। जल संरक्षण, स्वच्छता, और संगठित जल प्रबंधन जैसे उपाय अपनाकर हम इस संकट से निपट सकते हैं और एक स्थायी भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जल है तो कल है – इस बात को समझकर हमें जल संरक्षण के प्रति सजग होना होगा।
source – UNICEF,wikipedia
Manali Upadhyay
prakritiwad.com